उत्तराखंड का रिंगाल क्राफ्ट : परंपरा, संस्कृति और
अर्थव्यवस्था का संगम
प्रस्तावना
उत्तराखंड, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, केवल अपनी
प्राकृतिक सुंदरता, मंदिरों
और धार्मिक आस्था के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ की समृद्ध
सांस्कृतिक धरोहर और हस्तशिल्प परंपराएँ भी इसकी पहचान
हैं। पहाड़ के लोगों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, लेकिन उनकी
आत्मनिर्भरता और हुनर ने इन्हें हमेशा जीवित रखा है। इन्हीं पारंपरिक कलाओं में से
एक है रिंगाल
क्राफ्ट (Ringal
Craft)।
रिंगाल, बांस की एक विशेष प्रजाति है, जो उत्तराखंड
के ऊँचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इससे बनने वाले हस्तशिल्प न केवल ग्रामीण जीवन
का अभिन्न हिस्सा हैं, बल्कि आज यह कला पर्यावरण-संरक्षण
और स्थानीय अर्थव्यवस्था दोनों में अहम भूमिका निभा रही है।
रिंगाल
क्या है?
रिंगाल एक प्रकार का बौना बांस (dwarf bamboo) है। यह सामान्य
बांस से छोटा, पतला
और अधिक लचीला होता है।
- ऊँचाई
पर उगता है – यह
1000 से
3000 मीटर
की ऊँचाई पर पाया जाता है।
- भौगोलिक
क्षेत्र – कुमाऊँ
और गढ़वाल के पर्वतीय अंचल में रिंगाल का प्राकृतिक आवास है।
- विशेषताएँ – रिंगाल
हल्का, मजबूत, टिकाऊ
और आसानी से मुड़ने वाला होता है।
- स्थानीय
नाम – कुछ
क्षेत्रों में इसे निंगाव या निंगल भी
कहा जाता है।
यही कारण है कि पहाड़ी लोग सदियों से इसका उपयोग घरेलू वस्तुएँ
बनाने और सामाजिक अवसरों पर करते आ रहे
हैं।
ऐतिहासिक
पृष्ठभूमि
रिंगाल क्राफ्ट की परंपरा उतनी ही पुरानी है
जितनी पहाड़ की सभ्यता।
- पहले
जब आधुनिक प्लास्टिक या धातु की वस्तुएँ उपलब्ध नहीं थीं, तब रिंगाल
ही जीवन का आधार था।
- खेती-बाड़ी, अनाज
रखने, विवाह
समारोह, धार्मिक
अनुष्ठान, यहाँ
तक कि रोज़मर्रा की छोटी-बड़ी जरूरतों में रिंगाल
से बनी टोकरियाँ, चंगेर, सुपा और
दोक्का ही
उपयोग में आते थे।
- उत्तराखंड
की कई लोककथाओं और लोकगीतों में भी रिंगाल और इससे बनी वस्तुओं का उल्लेख
मिलता है।
इससे स्पष्ट है कि रिंगाल केवल एक पौधा नहीं, बल्कि समाज और
संस्कृति की पहचान है।
रिंगाल
क्राफ्ट की तकनीक और निर्माण प्रक्रिया
(क)
कच्चा माल इकट्ठा करना
- अक्टूबर-नवम्बर
में रिंगाल काटा जाता है।
- इसे
छाँटकर घरों या कार्यस्थलों तक लाया जाता है।
(ख)
सुखाना
- रिंगाल
को धूप में सुखाकर उसकी नमी निकाली जाती है।
- सुखाने
के बाद यह अधिक टिकाऊ हो जाता है।
(ग)
फाड़ना और पतली पट्टियाँ बनाना
- तेज
धारदार चाकू से इसे लंबाई में फाड़कर पतली-पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं।
- इन्हीं
पट्टियों को
warp और weft की
तरह इस्तेमाल किया जाता है।
(घ)
बुनाई
- विभिन्न
डिज़ाइन और तकनीकों से बुनाई की जाती है।
- तयल
(Tyal) नामक
तकनीक विशेष रूप से टिकाऊपन के लिए उपयोग होती है।
(ङ)
सजावट और रंगाई
- पारंपरिक
रूप में प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था।
- अब
आधुनिक बाजार की मांग के अनुसार चमकीले रंग और डिज़ाइन भी जोड़े जाते हैं।
रिंगाल
से बनने वाले उत्पाद
(क)
परंपरागत उत्पाद
- टोकरियाँ
(Tokari) – फल, सब्ज़ी, अनाज
ढोने के लिए।
- सुपा – अनाज
साफ करने के लिए।
- चंगेर – रसोई
में उपयोगी।
- दोक्का – अनाज
रखने की बड़ी टोकरी।
- चटाइयाँ
और थालियाँ – घरेलू
उपयोग में।
(ख)
आधुनिक उत्पाद
- लैंपशेड
- पेन
स्टैंड और डस्टबिन
- बैग
और पर्स
- फोटो
फ्रेम, फूलदान
और सजावटी बॉक्स
- संगीत
वाद्य यंत्र
इस तरह रिंगाल
उत्पाद अब केवल ग्रामीण जीवन तक सीमित नहीं, बल्कि सजावटी और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुँच चुके
हैं।
सांस्कृतिक
और सामाजिक महत्व
- उत्तराखंड
के विवाह समारोह में रिंगाल की बनी टोकरियाँ और सुपा आज भी परंपरा का हिस्सा
हैं।
- त्योहारों
में महिलाएँ इनका उपयोग करती हैं।
- कई
ग्रामीण समुदायों की पहचान ही रिंगाल शिल्प से होती है।
- यह
कला केवल वस्तुएँ बनाने की नहीं, बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी
हस्तांतरित होती परंपरा है।
आर्थिक
महत्व और स्थानीय व्यवसाय
- उत्तराखंड
में करीब
10,000 कारीगर सीधे
तौर पर इससे जुड़े हैं।
- ग्रामीण
परिवारों के लिए यह अतिरिक्त आय का साधन है।
- पर्यटन
स्थलों (जैसे मसूरी,
नैनीताल,
ऋषिकेश) पर रिंगाल उत्पादों की अच्छी बिक्री होती है।
- यह
पर्यावरण-सुरक्षित है,
इसलिए इसे प्लास्टिक का विकल्प माना
जा रहा है।
सरकारी
योजनाएँ और संस्थागत सहयोग
- उत्तराखंड
बांस एवं फाइबर विकास परिषद (UBFDB) – कारीगरों को प्रशिक्षण और विपणन
सहयोग।
- NGOs और
स्वयं सहायता समूह – महिलाओं और अनुसूचित जाति समुदायों को
जोड़ना।
- हुनर
हाट और मेले – कारीगरों
को प्रदर्शन का अवसर।
- प्रधानमंत्री
स्वरोजगार योजनाएँ – स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता।
चुनौतियाँ
1.
युवा पलायन – युवा पीढ़ी इस
कला में रुचि नहीं ले रही।
2.
बाजार की कमी – उत्पाद गाँव तक
ही सीमित रह जाते हैं।
3.
GI टैग का अभाव – इसे अभी तक राष्ट्रीय या
अंतरराष्ट्रीय पहचान नहीं मिली।
4.
प्रतिस्पर्धा – प्लास्टिक और
मशीन से बने सामान सस्ते हैं।
5.
सरकारी योजनाओं का अभाव या पहुंच न
होना।
समाधान
और भविष्य की संभावनाएँ
- रिंगाल
क्राफ्ट को GI टैग- उत्तराखंड
में हस्त शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में रिंगाल क्राफ्ट को जी. आई.
टैग (भौगोलिक संकेतक) प्राप्त हुआ है। प्रदेश में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भर
उत्तराखण्ड के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए रिंगाल के उत्पादों को GI Tag प्राप्त हुआ है
। आपको बता दें कि जी. आई. टैग भौगोलिक संकेत का संक्षिप्त रूप है किसी भी छेत्र , शहर या राज्य
की एक विशिष्ट पहचान है ,टैग
कुछ विशेष उत्पादों या संकेतों के नाम पर दिया जाता है जो कि उस छेत्र की
विशिष्टता का प्रतीक है ।
यह जी. आई. टैग भारत में माल से संबंधित भौगोलिक संकेतों के पंजीकरण और बेहतर सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करता है। अधिनियम का संचालन महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और व्यापार चिह्न द्वारा किया जाता है - जो भौगोलिक संकेतकों के रजिस्ट्रार हैं।
- डिजिटल
मार्केटिंग और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (Amazon, Flipkart, Etsy आदि)
पर बिक्री बढ़ाना।
- पर्यटन
उद्योग के साथ जोड़कर होटलों और रिसॉर्ट्स में सजावटी
उपयोग।
- युवाओं
को आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन और फैशन इंडस्ट्री से
तालमेल।
- ‘वोकल
फॉर लोकल’ और आत्मनिर्भर
भारत अभियान
के तहत प्रोत्साहन।
निष्कर्ष
रिंगाल क्राफ्ट केवल एक हस्तशिल्प नहीं, बल्कि उत्तराखंड की
आत्मा और पहचान है। यह परंपरा सदियों से लोगों के जीवन का हिस्सा
रही है और आज भी रोजगार, संस्कृति और
पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे रही है।
यदि इसे आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़ा जाए, तो यह न केवल
पहाड़ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएगा, बल्कि पूरे देश और विश्व में उत्तराखंड की
संस्कृति को नई पहचान देगा।

.jpeg)
.jpeg)


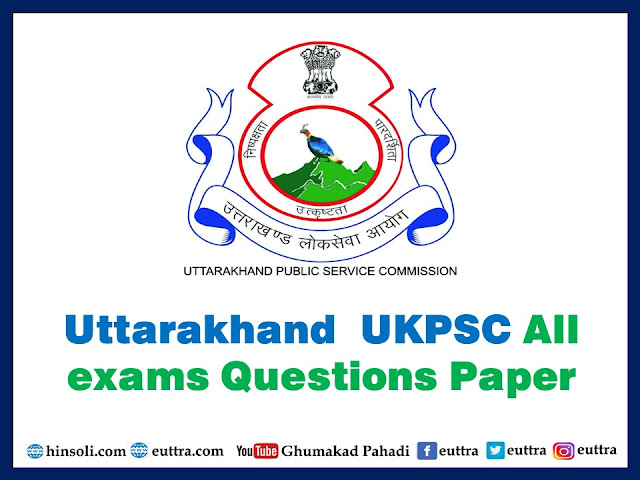

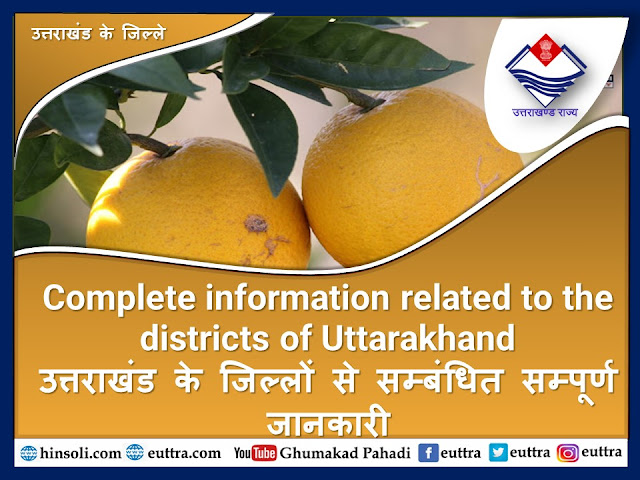


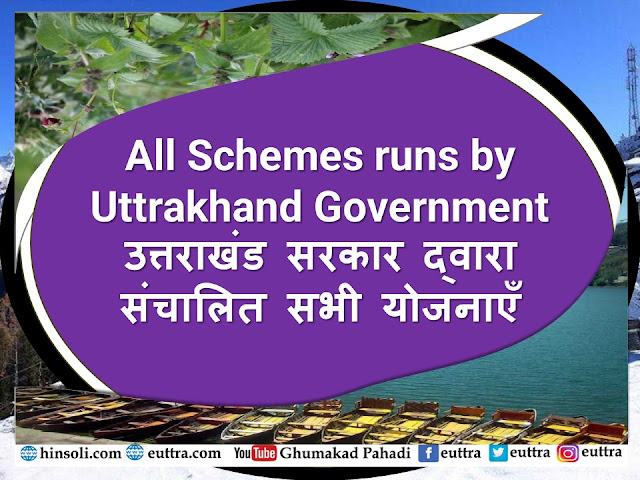






















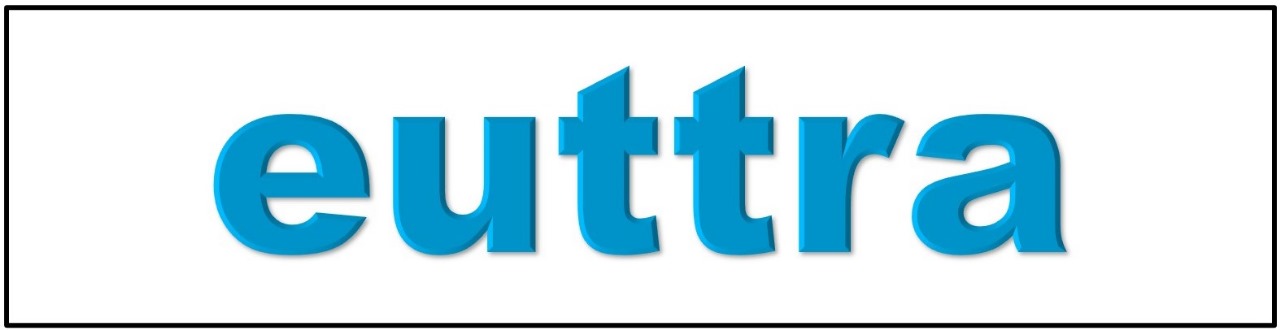
Follow Us